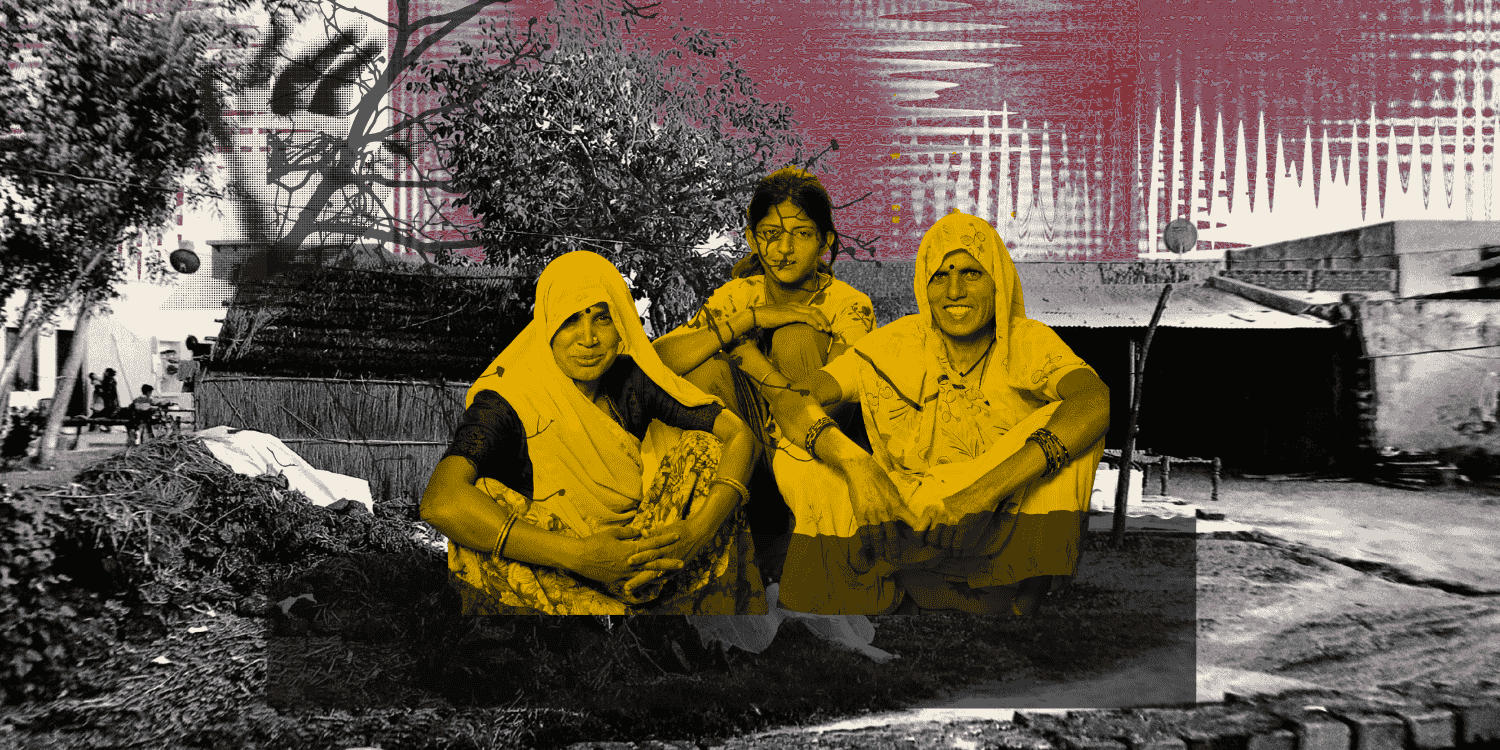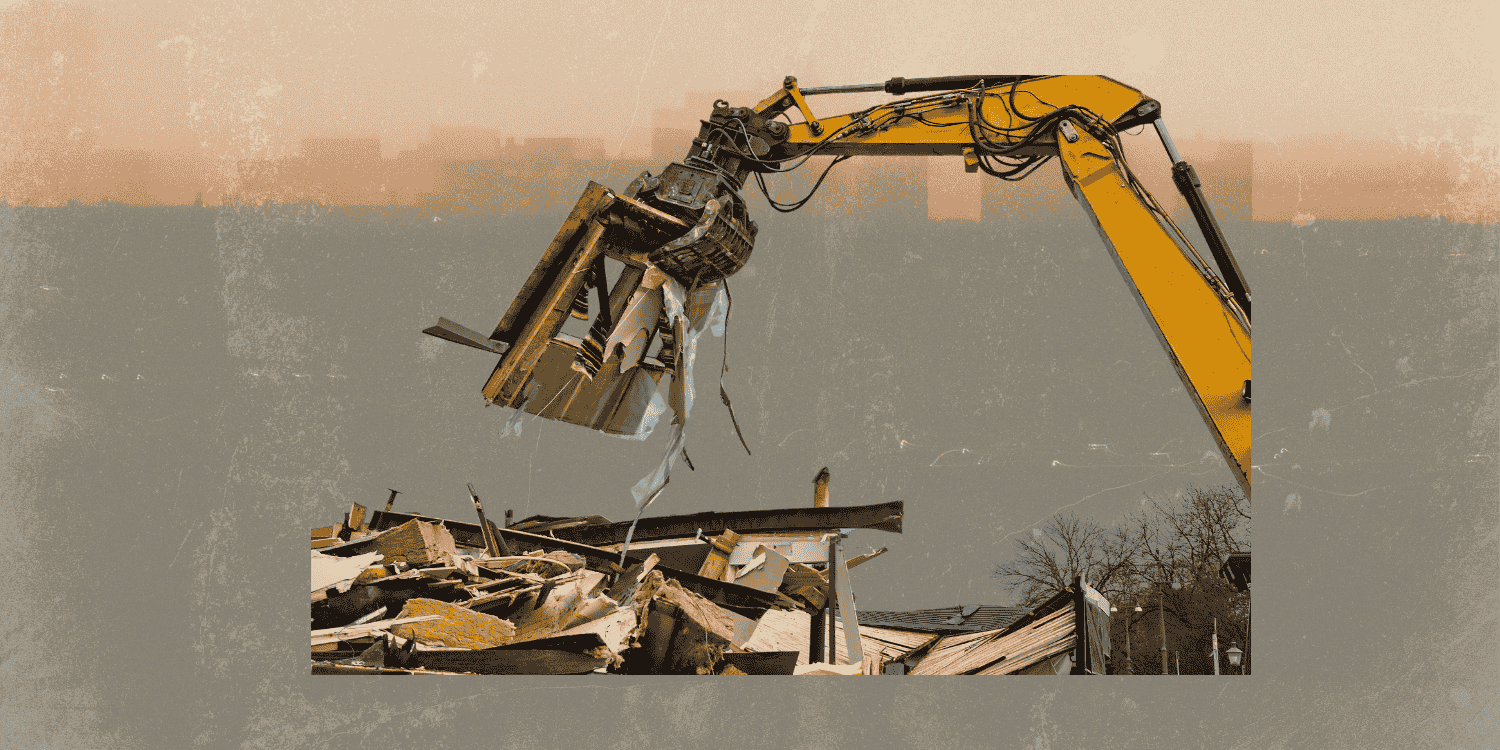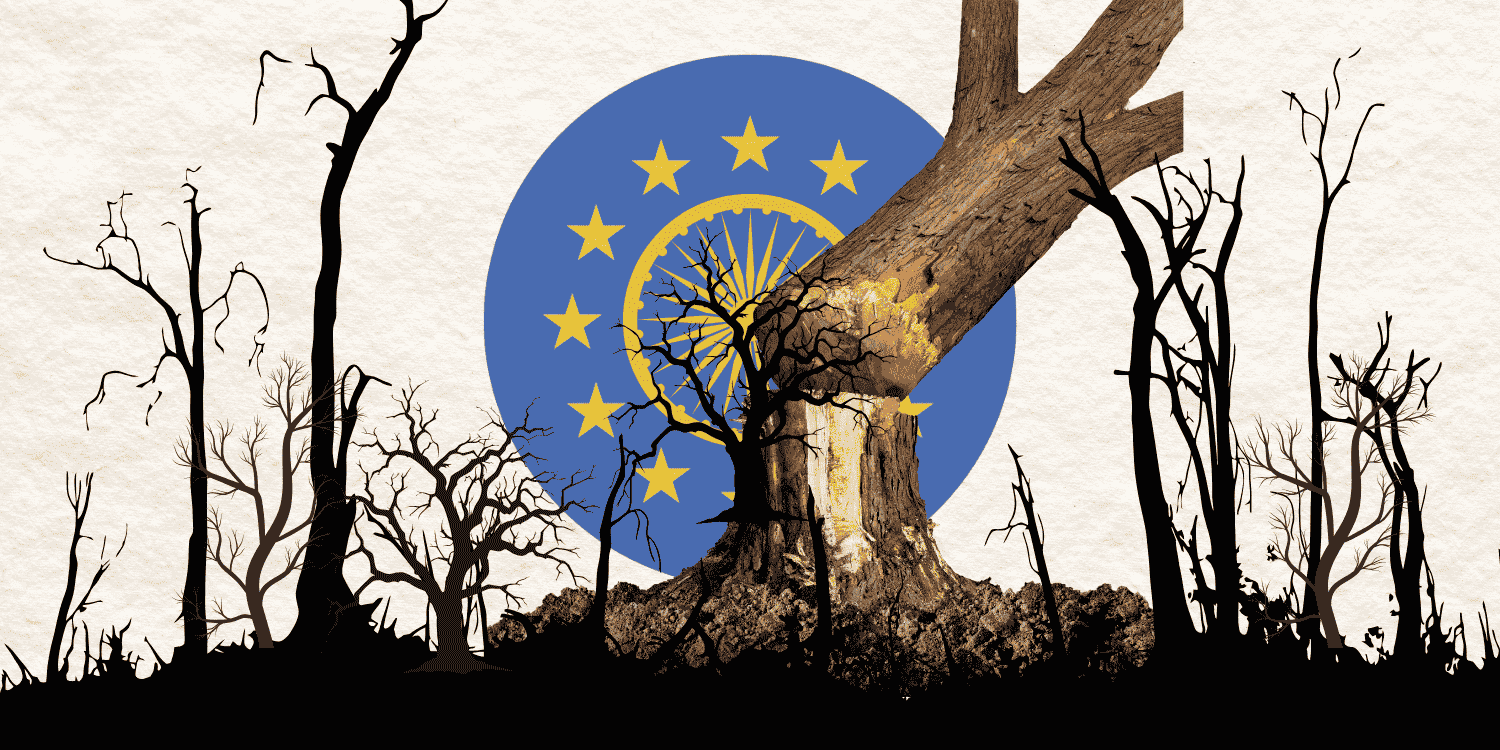उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक विवाह, तलाक, लिव-इन, उत्तराधिकार और बच्चों को गोद लेने के कानून में एकरूपता लाने का प्रयास है ताकि इसे सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 44 में पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। समान नागरिक संहिता या यूनिफार्म सिविल कोड को देश भर में लागू करने की बात काफी अरसे से की जा रही है लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से इसे एक नई शक्ल प्रदान की गई है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। वह पहले की तरह अपने रीति-रिवाज के अनुसार चलेंगे।
लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की अनिवार्यता
बिना शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को यदि एक छत के नीचे रहना है तो उन्हें साथ रहने पर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सहवासी होने के एक माह के अंदर रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर उत्तराखंड सरकार ने लिव-इन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की युवती और 21 वर्ष से अधिक आयु का युवक यदि बिना विवाह के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें इस नए कानूनी प्रावधान का पालन करना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर तीन माह के कारावास या अधिकतम दस हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता की धारा 387 में यह भी कहा गया है कि गलत या झूठी सूचना देने पर तीन माह की जेल और 25 हजार रुपए तक के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। लिव-इन रिश्तों की जानकारी नहीं देने पर छह माह तक के कारावास या 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का भागी बनना पड़ेगा।
लिव-इन के यह कठोर प्रावधान निजता और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों पर सीधी चोट करते हैं। लिव-इन का मतलब ही विवाह के बंधन से दूर रहना है। इसे पश्चिम की सभ्यता कहें या देश की युवा पीढ़ी का झुकाव-लिव-इन का चलन देश के हर भाग में तेजी से बढ़ा है। आधुनिक युग में महानगरों में यह चलन बहुत सामान्य हो गया है। घरेलू हिंसा कानून में सुप्रीम कोर्ट लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान कर चुका है। उत्तराखंड के लिव-इन पर बने कठोर प्रावधान संविधान की कसौटी पर खरे उतरेंगे या नहीं, यह देखना होगा। दो वयस्कों के बीच आपसी रजामंदी से बनाए गए संबंध किसी भी सूरत में अपराध की परिधि में नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 पर दिए अपने फैसले पर सहमति के आधार पर बनाए गए शारीरिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया था। लिव-इन रिलेशनशिप भी व्यक्ति की स्वायतत्ता और निजता के संवैधानिक अधिकार पर टिकी हुई है। पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। लिव-इन पर उत्तराखंड सरकार का नजरिया कानूनविदों को जरूर खटकेगा।
यूसीसी की धारा 388 के तहत लिव-इन से अलग हुई महिला को गुजारा भत्ता देने का भी प्रावधान है। लिव-इन के पार्टनर जिस जगह पर अंतिम बार साथ रहे, उसी क्षेत्राधिकार में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से भरण-पोषण की गुहार लगा सकती है। लिव-इन रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को वैध संतान का दर्जा हासिल होगा। यह एक प्रगतिशील प्रावधान है।
भारत में अभी भी विवाह का पंजीकरण नहीं कराने पर दंड देने का कानून नहीं है। इसलिए लिव-इन का रजिस्ट्रेशन खटकता है। एक तरफ शादी की न्यूनतम उम्र 18 और 21 तय की गई है। लिव-इन में दाखिल होने के लिए भी यही उम्र निर्धारित की गई है। लेकिन धारा 385 के अनुसार यदि महिला या पुरुष में से किसी की भी उम्र 21 वर्ष से कम है तो उसके माता-पिता को भी उनके लिव-इन रिलेशनशिप की सूचना दी जाएगी। उम्र की यह बाध्यता विरोधाभासी है। इसमें निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है। लिव-इन संबंध खत्म करने पर रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी होगी।
समान नागरिक संहिता का हिंदुओं पर प्रभाव
समान नागरिक संहिता के लागू होने से हिंदुओं के उत्तराधिकार और वारिसाना अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बदल जाएंगे। समान नागरिक संहिता में पुश्तैनी और स्वयं अर्जित की गई सम्पत्ति में भेद खत्म कर दिया गया है। नए कानून में हमवारिसों के अधिकारों की चर्चा नहीं है। हिंदुओं के संयुक्त परिवार मिताक्षरा कानून के तहत उत्तराधिकार निर्धारित करते हैं। पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, प्रपौत्र-प्रपौत्री को जन्म से ही सम्पत्ति का संयुक्त मालिकाना हक दिया जाता है। यह सभी हमवारिस माने जाते हैं। इसका मतलब है कि पिता पुश्तैनी सम्पत्ति को अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता, यदि उसकी संतान या वंशज जीवित हैं। पैत्रक सम्पत्ति को चार पुश्तों तक संयुक्त रूप से रखा जा सकता है। लेकिन स्वयं अर्जित की गई सम्पत्ति को पिता किसी को भी बेच सकता है।
बिना वसीयत की सम्पत्ति को मालिकाना हक तय करने में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत नियम निर्धारित हैं। इसमें माता को प्रथम श्रेणी के वारिसों में स्थान मिला है जबकि पिता को द्वितीय श्रेणी का वारिस माना गया है। मौजूदा उत्तराधिकार कानून के तहत बिना वसीयत की सम्पत्ति में मृतक के बच्चों, विधवा और मां का बराबर का हिस्सा होता है। इसमें पिता की जगह नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी में पिता और माता को समकक्ष रखा गया है। यानी बच्चों, विधवा, मां के साथ पिता की भी सम्पत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी। यदि प्रथम श्रेणी के वारिस मौजूद नहीं है तो फिर द्वितीय श्रेणी के वारिस सम्पत्ति के हकदार होंगे। हिंदू अविभाजित परिवार को मिलने वाले कर-लाभ पर भी समान नागरिक संहिता खामोश है।
समान नागरिक संहिता का मुसलमानों पर प्रभाव
समान नागरिक संहिता में हर धर्म के अनुयायियों के लिए शादी की उम्र एकसमान कर दी गई है। शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 और लडक़ी के लिए यह 18 है। हिंदुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत उम्र की यह सीमा पहले से निर्धारित है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह की उम्र 13 साल है। 13 साल की अवस्था को यौवन में प्रवेश की उम्र मानी गई है और इसीलिए सयानपन में ही शादी जायज मानी गई है। हालांकि पोक्सो और बाल विवाह अधिनियम के तहत नाबालिगों की शादी को अवैध बताया गया है। इसलिए मुस्लिम लॉ के तहत 13 साल की उम्र में निकाह की अनुमति देश के विभिन्न कानूनों के विपरीत थी।
सम्पत्ति के बंटवारे भी अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं हो पाएंगे। वसीयत या बिना वसीयत के उत्तराधिकार कानूनों में परिवर्तन किया गया है। इस समय, मुसलमान व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का अधिकतम एक तिहाई किसी को भी वसीयत के जरिए दे सकता है। जहां वसीयत नहीं है, वहां कुरान औ हदीस के अनुसार सम्पत्ति का बंटवारा होता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी वारिस सम्पत्ति के हक से वंचित नहीं रहे। लेकिन नए समान नागरिक संहिता कानून के तहत वसीयत में सम्पत्ति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नए कानून के तहत व्यक्ति वसीयत के जरिए कितनी भी सम्पत्ति किसी के भी नाम कर सकता है।
बहुविवाह, निकाह हलाला और इद्दत को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। एक पत्नी के जीवित रहते हुए, दूसरा निकाह अवैध है। तलाक के बाद मुसलमान दूसरा विवाह कर सकता है। समान नागरिक संहिता की धारा 32 के तहत कानून का उल्लंघन करके निकाह करने वाले को तीन साल की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है।
समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के अलावा उन पर भी लागू होगी जो वहां से ताल्लुक रखते हैं या उनमें से कोई एक किसी अन्य राज्य में भी रहता है। उत्तराखंड के बाद असम ने भी समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाए हैं। असम में यह किस सूरत में सामने आएगा, अभी स्पष्ट नहीं है।